पाकिस्तान की भाषाएँ
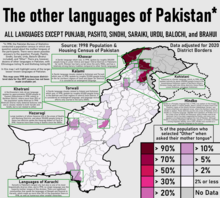
पाकिस्तान में कई दर्जन भाषाएँ बोली जाती हैं। निम्नलिखित पाँच भाषाओं में प्रत्येक के 1 करोड़ से अधिक वक्ता हैं — पञ्जाबी, पश्तो, सिन्धी, सरायकी और उर्दू। पाकिस्तान की लगभग सभी भाषाएँ भारोपीय भाषा परिवार के भारत-ईरानी समूह से सम्बन्धित हैं।
उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है और इसके साथ-साथ अँग्रेजी भी पाकिस्तान की सह-राजभाषा है। पाकिस्तान के विभिन्न समूहों द्वारा उर्दू को सम्पर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। [उद्धरण वांछित]
एथनोलॉग ने पाकिस्तान में 74 भाषाओं को सूचीबद्ध किया है। इनमें से 66 स्वदेशी हैं और 8 विदेशी हैं। उनकी जीवन शक्ति के सन्दर्भ में, 6 को 'संस्थागत', 18 को 'विकासशील', 39 को 'हष्ट-पुष्ट', 9 को 'परेशानी' में और 2 को 'मर' रही भाषाओं रूप में वर्गीकृत किया गया है।
राजभाषा
[संपादित करें]उर्दू (राजभाषा)
[संपादित करें]
उर्दू भाषा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा एवं पाकिस्तान की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है।[1] हालाँकि केवल 7% पाकिस्तानी ही इसे अपनी प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं। उर्दू बहुत-से पाकिस्तानियों के द्वारा दूसरी भाषा के रूप में बोली और समझी जाती है और नगरीय पाकिस्तानियों द्वारा इसे प्रथम भाषा के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है। [उद्धरण वांछित]
1947 में नये पाकिस्तान-राज्य के लिए एकता के प्रतीक के रूप में उर्दू को चुना गया क्योंकि यह पहले से ही उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के बीच आम भाषा के रूप में काम कर रही थी।[2]
उर्दू को अँग्रेजी और उर्दू माध्यम दोनों विद्यालय प्रणालियों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसके कारण ऐसे लाखों लोग उर्दू भाषा बोलने लगे हैं जिनकी मूल भाषा उर्दू नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उर्दू ने पाकिस्तान की विभिन्न क्षेत्रीय/प्रान्तीय भाषाओं की शब्दावली को आत्मसात किया गया है; इसके विपरीत भी यह हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं ने भी उर्दू की शब्दावली को आत्मसात किया है।
अँग्रेजी (सह-राजभाषा)
[संपादित करें]अँग्रेजी भाषा पाकिस्तान की सह-आधिकारिक भाषा है और इसे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के साथ-साथ पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के अधिकारी रैङ्क में भी उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान का संविधान और विधियाँ अँग्रेजी में लिखे गए्ये थे और अब उन्हें स्थानीय भाषाओं में फिर से लिखा जा रहा है। इसे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
अन्य भाषाएँ
[संपादित करें]अरबी
[संपादित करें]अरबी आधिकारिक भाषा थी। जब पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य का क्षेत्र 651 ई॰ और 750 ई॰ के बीच उमय्यद खिलाफ़त का हिस्सा था।
पाकिस्तान के संविधान में अरबी का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 31 संख्या 2 में घोषणा करता है कि "पाकिस्तान के मुसलमानों के सम्बन्ध में राज्य प्रयास करेगा (ए) पवित्र कुरान और इस्लामियत की शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये, अरबी भाषा सीखने को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए ..."[3]
अरबी भाषा मुसलमानों की पान्थिक (Religious) भाषा है। कुरान, सुन्नत, हदीस और मुस्लिम पान्थिक पुस्तकें अरबी में उर्दू अनुवाद के साथ पढ़ायी जाती है। पश्चिमी एशिया में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों ने पाकिस्तान में अरबी बोलने वाले लोगों की संख्या में और वृद्धि की है। अरबी को मस्जिदों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और मदरसों में पान्थिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या ने अपनी पान्थिक शिक्षा के हिस्से के रूप में अरबी के पढ़ने, लिखने और उच्चारण में औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 अनुच्छेद 3.7.4 घोषित करती है कि: "अरबी भाषा को अनिवार्य भाग के रूप में इस्लामियत में मध्य से उच्च माध्यमिक स्तर तक जोड़ा किया जायेगा ताकि छात्रों को कुरान को समझने में सक्षम बनाया जा सके।" इसके अलावा, यह अनुच्छेद 3.7.6 में निर्दिष्ट करती है: "ऐच्छिक विषय के रूप में अरबी भाषा को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अरबी साहित्य और व्याकरण के साथ ठीक से प्रस्तुत किया जायेगा ताकि शिक्षार्थियों को भाषा में अच्छी पकड़ मिल सके।" यह विधि निजी विद्यालयों के लिए भी मान्य है क्योंकि यह अनुच्छेद 3.7.12 में परिभाषित करता है: "इस्लामियत, अरबी भाषा और सार्वजनिक क्षेत्र की नैतिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को निजी संस्थानों द्वारा समाज में एकरूपता बनाने के लिये अपनाया जायेगा।"[4]
फ़ारसी (ऐतिहासिक आधिकारिक एवं साहित्यिक भाषा)
[संपादित करें]फ़ारसी भाषा मुगल साम्राज्य की आधिकारिक व सांस्कृतिक भाषा थी। जो मध्य एशियाई तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा भाषा की शुरुआत के बाद से एक निरन्तरता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में चले गये थे, और पहले तुर्को-फ़ारसी दिल्ली सल्तनत द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। अंग्रेजों के आगमन के साथ फ़ारसी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था: 1843 में सिन्ध में और 1849 में पंजाब में। यह आज मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान से दारी बोलने वाले शरणार्थियों और स्थानीय बलूचिस्तानी हज़ारा समुदाय की एक छोटी संख्या द्वारा बोली जाती है, जबकि अधिकांश पाकिस्तानी हज़ारा हजारागी बोलते हैं। जिसे कुछ विशेषज्ञ एक अलग भाषा मानते हैं और दूसरों द्वारा विभिन्न प्रकार की फ़ारसी भाषा माना जाता है।
बंगाली भाषा (गत क्षेत्रीय व अप्रवासी भाषा)
[संपादित करें]बंगाली भाषा पाकिस्तान में एक आधिकारिक भाषा नहीं है, किन्तु पाकिस्तानी नागरिकों की एक बड़ी संख्या पूर्वी बंगाल से पलायन कर गयी थी, जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे। बंगाली भाषा को 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गयी थी, और पाकिस्तान के संविधान के 214 (1) में पुनः लिखा गया कि "पाकिस्तान की राज्य भाषा उर्दू और बंगाली होगी"। अन्य व्यक्ति जिसमें कि अवैध अप्रवासी भी शामिल हैं जो 1971 के बाद बांग्लादेश से पलायन कर गये थे। अधिकांश पाकिस्तानी बंगाली और पाकिस्तानी बिहारी (उर्दू और बंगाली) द्विभाषी हैं, और मुख्य रूप से कराची में बसे हैं।
तुर्क भाषाएँ (ऐतिहासिक व अप्रवासी भाषाएँ)
[संपादित करें]तुर्क भाषाओं का उपयोग मुगलों और उपमहाद्वीप के पूर्व के सुल्तानों जैसे तुर्को-मंगोलों द्वारा किया जाता था। पूरे देश में तुर्किस बोलने वालों के छोटे-छोटे हिस्से पाये जाते हैं, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में घाटियों में, जो मध्य एशिया से सटे हुए हैं, पश्चिमी पाकिस्तानी का वज़ीरिस्तान क्षेत्र मुख्य रूप से कनिगोरम के आसपास, जहाँ बुर्की जनजाति निवास करती है और पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के नगरीय केन्द्रों में हैं। मुगल राजा बाबर की आत्मकथा तुज़क बाबरी भी तुर्की भाषा में लिखी गयी थी। 1555 में सफ़विद फ़ारस में निर्वासन से लौटने के बाद, मुगल राजा हुमायूँ ने आगे फारसी भाषा और संस्कृति को न्यायालय और राजकीय कार्यों में प्रस्तुत किया। चगताई भाषा, जिसमें बाबर ने अपने संस्मरण लिखे थे, दरबारी कुलीन वर्ग की संस्कृति से लगभग पूरी तरह से गायब हो गयी, और मुगल राजा अकबर इसे नहीं बोल सका। कहा जाता है कि बाद के जीवन में, हुमायूँ ने स्वयं फ़ारसी पद्य में अधिक से अधिक बार बात की थी।
अंग्रेजी (गत औपनिवेशिक एवं सह-आधिकारिक भाषा)
[संपादित करें]अंग्रेजी पाकिस्तान की एक सह-आधिकारिक भाषा है और व्यापक रूप से कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के साथ-साथ पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के अधिकारी रैंक में कुछ सीमा तक उपयोग की जाती है। पाकिस्तान का संविधान और विधि अंग्रेजी में लिखे गये थे और अब स्थानीय भाषाओं में पुनः लिखे जा रहे हैं। यह शिक्षा के माध्यम के रूप में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। अंग्रेजी को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की भाषा के रूप में देखा जाता है, और इसका उपयोग ऊपरी सामाजिक वर्ग में अधिक प्रचलित हो रहा है, जहाँ इसे बहुधा देशी पाकिस्तानी भाषाओं के साथ बोला जाता है। 2015 में, यह घोषणा की गयी थी कि आधिकारिक व्यवसाय में उर्दू को बढ़ावा देने की योजना थी, किन्तु पाकिस्तान के योजना मन्त्री अहसान इकबाल ने कहा, "उर्दू भाषा का दूसरा माध्यम होगा और सभी आधिकारिक व्यवसाय द्विभाषी होंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों में उर्दू के साथ-साथ अंग्रेजी भी पढ़ायी जायेगी।[5]
विदेशी भाषाएँ
[संपादित करें]2017 तक, कुछ पाकिस्तानी चीनी जनवादी गणराज्य की कम्पनियों के साथ व्यापार करने के लिये चीनी भाषा सीख रहे हैं।[6]
सांख्यिकी
[संपादित करें]| भाषा | 2008 का अनुमान | 1998 जनगणना | कहाँ बोली जाती है | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पंजाबी | 76,367,360 | 44.17% | 58,433,431 | 44.15% | पंजाब | |||
| 2 | पश्तो | 26,692,890 | 15.44% | 20,408,621 | 15.42% | खैबर-पख़्तूनख्वा | |||
| 3 | सिन्धी | 24,410,910 | 14.12% | 18,661,571 | 14.10% | ग्रामीण सिन्ध | |||
| 4 | सराइकी | 18,019,610 | 10.42% | 13,936,594 | 10.53% | पंजाब | |||
| 5 | उर्दू | 13,120,540 | 7.59% | 10,019,576 | 7.57% | सिन्ध के नगरों एवं पाकिस्तान के नगरों में | |||
| 6 | बलोची | 6,204,540 | 3.59% | 4,724,871 | 3.57% | बलूचिस्तान | |||
- सन १९५१ और १९६१ की जनगणना में सराइकी बोली पंजाबी के साथ रखी गयी थी।
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 251
- ↑ https://epaper.dawn.com/DetailImage.php?StoryImage=25_12_2017_116_001
- ↑ https://pakistanconstitutionlaw.com/article-31-islamic-way-of-life
- ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 10 जनवरी 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 नवंबर 2021.
- ↑ http://tribune.com.pk/story/928480/pakistan-to-replace-english-with-urdu-as-official-language/
- ↑ https://www.dw.com/en/why-are-pakistanis-keen-to-learn-chinese-language/a-41465711
