ज्वारबंधन
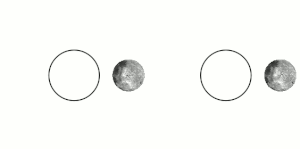

खगोलशास्त्र में ज्वारबंधन (tidal locking, gravitational locking) उस स्थिति को कहते हैं जब अपनी कक्षा (ऑरबिट) में परिक्रमा करती हुई किसी खगोलीय वस्तु और उसके गुरुत्वाकर्षक साथी के बीच कोणीय संवेग (angular momentum) की अदला-बदली नहीं होती। साधारणतः इस स्थिति में वह वस्तु अपने साथी की ओर एक ही मुख रखती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण पृथ्वी का चंद्रमा है जो पृथ्वी के साथ ज्वारबंध है और पृथ्वी की तरफ़ उसका एक ही मुख रहता है, जिस कारण से पृथ्वी से उसका केवल एक ही मुख दिखता है और उसका उल्टा मुख देखने के लिए पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष यान से चंद्रमा के पीछे जाना होता है।[1][2]
कारण व प्रभाव[संपादित करें]
जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की परिक्रमा करती है तो वे एक दूसरे पर ज्वारभाटा बल का प्रभाव डालती हैं, जिस से धीरे-धीरे उनका घूर्णन काल (रोटेशन) और कक्षीय अवधि (रेवोल्यूशन) की दो अवधियाँ समान होती चली जाती हैं और अंततः ज्वारबंधन हो जाता है। यह छोटे आकार की वस्तु में तेज़ी से और बड़े आकार की वस्तु में धीरे-धीरे होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का पृथ्वी के साथ ज्वारबंध है लेकिन पृथ्वी का चंद्रमा के साथ अभी नहीं हुआ है। जब दोनों वस्तुओं का आकार एक-दूसरे के समीप हो तो दोनों में ही ज्वारबंध उत्पन्न हो जाता है। प्लूटो और उसके उपग्रह शैरन के बीच ऐसा है - प्लूटो का एक ही मुख शैरन के भी एक ही मुख के आमने-सामने सदैव के लिए अटका हुआ है।[3]
ज्वारबंध ग्रहों पर जीवन उत्पन्न होने की सम्भावनाओं पर खगोलशास्त्रियों में काफ़ी विवाद चल रहा है।[4]
घूर्णन-कक्षा अनुनाद[संपादित करें]
ऐसी स्थितियों में जब कक्षा विकेन्द्रित (eccentric) और ज्वारभाटा प्रभाव कमज़ोर हो तो छोटी वस्तु, सीधा ज्वाबंध होने की बजाय, घूर्णन-कक्षा अनुनाद (spin-orbit resonance) में आ सकती है। इसमें उस वस्तु के घूर्णन काल और उसकी कक्षीय अवधि के बीच एक सरल अनुपात (रेशो) देखा जाता है। मसलन बुध ग्रह का घूर्णन काल और उसकी सूरज के इर्द-गिर्द परिक्रमा की कक्षीय अवधि में 3:2 का अनुनाद है।
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ Barnes, Rory, संपा॰ (2010), Formation and Evolution of Exoplanets, John Wiley & Sons, पृ॰ 248, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 3527408967, मूल से 21 मार्च 2017 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 4 मार्च 2017.
- ↑ Heller, R.; एवं अन्य (April 2011), "Tidal obliquity evolution of potentially habitable planets", Astronomy & Astrophysics, 528: 16, arXiv:1101.2156, डीओआइ:10.1051/0004-6361/201015809, बिबकोड:2011A&A...528A..27H, A27.
- ↑ "When Will Earth Lock to the Moon?". Universe Today. मूल से 23 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 मार्च 2017.
- ↑ "Life on a tidally-locked planet" (PDF). Cornell University Library. मूल से 16 अप्रैल 2017 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 21 January 2017.
