इन दिनों
| इन दिनों | |
|---|---|
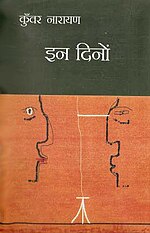 मुखपृष्ठ | |
| लेखक | कुँवर नारायण |
| देश | भारत |
| भाषा | हिंदी |
| विषय | साहित्य |
| प्रकाशक | राजकमल प्रकाशन |
| प्रकाशन तिथि |
२००२ |
कुंवर नारायण भारतीय परंपरा के उन प्रमुख कवियों में हैं जिनकी कविता मानवीय मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन और निर्माण के लिए किसी बड़ी नदी की तरह हर बार मार्ग बदलती रही है। उनता छठा कविता संग्रह इन दिनों पढ़ते हुए जीवन के पचहत्तर वर्ष पूरे करने वाले कवि के जीवनाभुवों से मिलने-टकराने की भी अपेक्षा रहती है। जीवन के अनेकानेक पक्षों को जिस भाषिक संक्षिप्तता और अर्थ गहराई के साथ उन्होंने कविता का विषय बनया है उसे देखकर उन्हीं की कविता पंक्ति में ‘कभी’ की जगह ‘कवि’ को रखकर कहा जा सकता है कि – ‘कवि तुमने कविता की ऊंचाई से देखा शहर’ और अब इस ताजा संग्रह में उन्होंने कहा है कि ‘बाजार की चौंधिया देने वाली जगमगाहट, के बीच / अचानक संगीत की एक उदास ध्वनि में हम पाते हैं / उसके वैभव की एक ज्यादा सच्ची पहचान’।
इन पंक्तियों में अर्थ की सारी चाभी ‘उदास’ विशेषण के पास है जिसका अन्वय बाजार, संगीत और ध्वनि तीनों के साथ करना पड़ेगा और समन्वय करना पड़ेगा ‘वैभव’ के साथ भी। इस संग्रह में कहीं किसी निरर्थक विशेषण का प्रयोग कवि ने नहीं किया है। इस सृजन संयम से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन कविताओं में यदि कोई खोट या मैल दिखाई दे तो वह रचनाकार की दुनिया में विनम्र न होकर जाने का अहंकार है जो शायद ‘सादगी’ कविता की इन पंक्तियों से तुष्ट हो सके : ‘तुम्हारे कपड़ों का दोष है / मिट्टी का नहीं / जो उसे छूते ही मैले हो गये तुम /’ शुरू से ही उनकी कविताओं में ‘अलख’ (जो दिखाई नहीं देता है। वह यथार्थ) दिखाने के प्रति विशेष रुझाम रहा है जिसे पुराने मुहावरे में ‘अलख जगाना’ कहते थे जो कहने को व्यक्तिगत नहीं रहने देता और सहने की दुर्निवार अभिव्यक्ति को सामाजिक बना देता है।
हम ऐसे समय में आ गये हैं जब बाजार वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का साधन और सूत्रधार बनकर आधुनिकता और विकास को उदास और प्रसन्न दो चेहरों की तरह धारण किये हुए सब पर छा गया है। कवियों के लिए भले ही यह स्थायी भाव न रहा हो, लेकिन हिंदी कविता में यह बाजार-भाव नया नहीं है। पिछले सात सौ साल से तो यह चल ही रह है। प्राचीन जगत व्यापार से लेकर ‘कबिरा घड़ा बाजार में’ और ‘धोति फटी सिलटी दुपटी’ से लेकर आज तक यह बाजार व्याप्त रहा है। बाजारवाद का जवाब देने के लिए आज जिस नयी दृष्ट की जरूरत है उससे उपजी हुई कविताएं कुंवर नारायण के इस नये कविता संग्रह में एकत्र हुई हैं। ‘इन दिनों’ में जो कुछ भी हमें घेरे, दबोचे और चिंतित किये हुए है वह किसी न किसी सूत्र के रूप में इस संग्रह की ८३ कविताओं में मौजूद है। इन कविताओं में दरअसल प्रेम के खो जाने का और बाजार के आतंक का मुकाबला मानवीय सहजता से व्यंग्य क्षमता के अनोखे अंदाज में किया गया है। न कवि ने स्वयं को कहीं परास्त माना है न विजेता, फिर भी जले हुए मकान की वास्तविकता के सामने अपने जीवित होने को कई कत्लों के बाद जीवित होना माना है। यह रूपक वहां तक जाता है जहां उसे कहना पड़ता है कि ‘ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, रुकते ही नहीं किसी तरह मेरी हत्या के सिलसिले।‘ यह जला हुआ मकान हिंदुस्तान के सिवा आखिर हो भी कौन सकता है? इतने बड़े मकान में एक छोटा घर और इस ‘घर का दरवाजा जैसे गर्द से ढंकी एक पुरानी किताब’, जिसमें ‘लौटी हो एक कहानी अपने नायक के साथ छानकर दुनिया भर की खाक’। ‘जो रोज पढ़ता है अखबारों में कि अब वह नहीं रहा, अपनी शोकसभाओं में खड़ा है वह, आंखें बंद किये – दो मिनटों का मौन।‘ इस भयावह समय में कुंवर नारायण का कविता संग्रह व्यक्तिगत डायरी, कहानी, निबंध और नाटक का मिलाजुला स्वाद देने वाले किसी अलभ्य ऐलबम की तह अपनी जीवंत उपस्थिति के घेरे में ले लेता है : ‘आधी रात अपने घर में घुस रह हूं चोरों की तरह/... मैं अपने सिरहाने खड़ा हूं अपने को सोता हुआ देखकर... मैं नहीं जानता कि मैं हत्यारा हूं या मेरी हत्या हुई है/ जब भी आईने के सामने पड़ता हूं चौंक जाता हू/ मेरी सूरत कभी एक से तो कभी दूसरे से मिलती है।‘
पूरा विश्व अलग-अलग शहरों में नहीं, बल्कि किसी एक ही शहर के विश्वव्यापी परिसर में रहता है जिसे कुतुब परिसर या किसी चिड़ियाघर की तरह काप्काई दृष्टि से देखा जा सकता है। बहुत सी घटनाएं २२ नंबर स्वर्णगली से लेकर वेनिस और बल्लीमारान, हैब्सबग्रज के भव्य महल या वावेल दुर्ग या लाल किले के दीवान-ए-ख़ास और अमीर खुसरो की एक नयी पहेली तक एक साथ एक ही परिसर में घटित हो जाती हैं। इन सबके कोलाज और गुंफन के लिए ‘काफ्का के प्राहा में’ की ये पंक्तियां बहुत सारी उद्भावनाओं और निष्कर्षों को एक साथ समेट लेती हैं : ‘कभी-कभी एक जिंदगा से ज्यादा अर्थपूर्ण हो सकती है/ उस पर टिप्पणियां/ एक प्रेम से ज्यादा मधुर हो सकती है उसकी स्मृतियां/ एक पूरी सभ्यती की वीरगाथाओं से कहीं अधिक सारगर्भित/ हो सकती है एक स्मारक की संक्षिप्त भाषा’
पेड़, चिड़िया, फूल, रंग और बच्चे अब भी कुंवर नारायण की कविताओं में पुरानी उम्मीदों की तरह बार-बार लौट आते हैं। ये बिंबों के रूप में नहीं बल्कि घटनाओं से लबरेज आत्मकथा के रूप में फिर कोई जन्म ले लेते हैं। सबके सुख-दुख नियति और परिणति की भाषा अपनी चिंता में यहां एक हो जाती है। उदासी और उल्लास का जन्मदिन एक साथ मन जाता है। एक पेड़ अगर आपका घनिष्ठ पड़ोसी हो तब आप समझ सकते हैं कि वह तो एक पूर्वज और दोस्त नहीं खुद हमारी तरह एक बेचैन प्राणी है। उसकी बांहों में चिड़ियों का बसेरा नहीं है, बल्कि उसने तो परे मकान को ही चिड़ियों के घोंसले में बदल दिया है। सारी ऋतुओं का पड़ाव वह वृक्ष घर के बाहर चौकीदार की तरह खड़ा है और वह तटस्थ नहीं है; अतीत और भविष्य में जाने का दरवाजा बन जाता है।
कुंवर नारायण की कविताओं की भाषा एक स्तर पर दार्शनिक चिंतन को उकसाती है और दूसरे स्तर पर मनोविश्लेषण की गति तेज कर देती है। कविता के संबंध में स्वयं कवि की धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में भी हम उनकी कविताओं को समझ सकते हैं : ‘…. जीवन के प्रति बेहतर समझ, संवेदनशीलता और न्यायबोध के अलावा कविता विचार वस्तु को भी अधिक कलापूर्ण- भावनात्मक और अधिक सरस ढंग से हमारे सामने रखती हैं, जैसा कि वह जीवन यथार्थ के साथ भी करती हैं। इस प्रकार देखें तो उच्च विचार उच्च कला से अलग नहीं, उसमें अंतर्निष्ठ होते हैं- औक कभी-कभी उसकी प्रेरणा भी बन सकते हैं। अच्छा विचार अच्छी कविता भी तभी हो सकेगा, जब दोनों एक दूसरे को खारिज कर देंगे।‘ यह तो कविता का काम है लेकिन उनके यहां तो कवि पर और कवि के काम पर भी एक पूरी कविता है : ‘बीमार नहीं है वह, कभी-कभी बीमार-सा पड़ जाता है/ उनकी खुशी के लिए जो सचमुच बीमार रहते हैं/ कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे/ अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं/ उनके कभी न मरने के भी उदाहरण हैं/ उनकी खुशी के लिए जो कभी नहीं मरते हैं।
उत्सर्गधर्मिता और जीवट के संबंध में उक्तियों और मुहावरों से बनी ऐसी कविता साहित्य में दुर्लभ है। राग, फाग और आग भी उनकी कविताओं में नयी संवेदना के साथ आते हैं। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच अपनी ऊर्जा को संगठित-निर्मित करते हैं इसीलिए उनकी कविता में कोई भी ऐतिहासिक, पौराणिक और मिथकीय फैंटेसी उसी सहजता के साथ आ जाती है जिस तरह कि प्रत्येक वस्तु में आग का होना बताया गया है। यह आग जब कविता के रूप में आती है तो फिर भले ही हमेशा एक नदी का किनारा वहां मौजूद हो, उसकी लपटें हमें तरह-तरह से पिघलाती, पकाती या झुलसाती रहती है। इसी बिंदु पर पहुंचकर कुंवर नारायण कहते हैं कि – ‘खेलूंगा आग से’। ऐसे वक्त यह एहसास हमें समूची समकालीनता के साथ उठाकर वर्तमान के पूरे इतिहास से जोड़ देता है जब कवि कहता है कि- ‘मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों-दिन क्षीण पड़ती जा रही है’। प्रत्यक्ष विरोध और उग्र घृणा अनेक मानवीय गुणों के सामने हमेशा कमजोर पड़ जात हैं और रचनाकारों की बनायी दुनिया में से आड़े वक्त शेक्सपीयर, गालीब, गुरू नानक, कंबन त्यागराज, मुत्तुस्वामी और प्रेम-रोग शब्द आते ही मीरा जैसे हाड़-मांस वाले व्यक्तित्व की सारी नफरत से लड़ने लगते हैं।
कुंवर नारायण की कविता एक ऐसी दुनिया रचती है जिस में रोज-रोज होती हत्याओं और सांप्रदायिक दुर्भावना के खिलाफ कवि मनुष्य के रूप में एक दागदार जीवन भी जीने को तैयार है, बशर्ते कि वह किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म हो। कहने की और बनाकर करने की जिद छोड़ते हुए कुंवर नारायण की इस संग्रह की कविताओं में जो तत्त्व ज्यादा छाया हुआ है वह ‘जख्म’ कविता से निस्सरित होता हुआ लगता है : ‘इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था/ और अगर दाग ही लगना था तो फिर/ कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं/ आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता/ जो कभी न मरता।‘ यहां स्थितियों को बदलने की तीव्र इच्छा और मनुष्य से नफरत न कर पाने के बीच का इन दिनों चलता सघर्ष भी कलात्मक ऊंचाइयों के साथ देखा जा सकता है।
