कन्नौज
| कन्नौज | |
|---|---|
| शहर | |
 माता अन्नपूर्ण मंदिर | |
| निर्देशांक: 27°04′N 79°55′E / 27.07°N 79.92°Eनिर्देशांक: 27°04′N 79°55′E / 27.07°N 79.92°E | |
| देश | |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| ज़िला | कन्नौज ज़िला |
| ऊँचाई | 139 मी (456 फीट) |
| जनसंख्या (2011) | |
| • कुल | 84,862 |
| भाषाएँ | |
| • प्रचलित | हिन्दी |
| समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+5:30) |
| वाहन पंजीकरण | UP-74 |
| वेबसाइट | www |
कन्नौज (IAST:Kannauj) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। शहर का नाम संस्कृत के कान्यकुब्ज (Kānyakubja) शब्द से बना है। कन्नौज एक प्राचीन नगरी है एवम् कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है।[1][2]
परिचय[संपादित करें]
कन्नौज स्पष्ट रूप से भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध नगर था।[3] और कन्नौज के चारों ओर के क्षेत्र को सामान्यतः आर्यावर्त कहा जाता था.[4]
कन्नौज गंगा के बायीं ओर ग्रैंड ट्रंक रोड से 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। किसी समय गंगा इस नगर के पार्श्व से बहती थी। रामायण में इस नगर का उल्लेख मिलता है। तॉलेमी ने ईसा के काल में कन्नौज को 'कनोगिज़ा' लिखा है। पाँचवीं शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। छठी शताब्दी में श्वेत हूणों के आक्रमण से यह काफी विनिष्ट हो गया था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग, ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इस नगर का उल्लेख किया है। 11वीं शताब्दी के आंरभिक काल में मुसलमानों के आक्रमण के कारण यह नगर काफी विनिष्ट हुआ। 1194 ई. में मुहम्मद गौरी ने इस नगर पर अपना स्वत्व जमाया। 'आइने अकबरी' द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर के समय में यहाँ सरकार का मुख्य कार्यालय था। प्राचीन काल के भग्नावशेष आज भी लगभग छह कि.मी. व्यास के अर्धवृत्तीय क्षेत्र में वर्तमान हैं। कन्नौज अपने मन्दिरो के लिये विशेष जाना जाता है। कन्नौज प्रमुख रुप से सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मन्दिर एवं सिद्धपीठ माँ फूलमती मंदिर के लिये जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ अनेकों मन्दिर हैं, जो की इस नगर की छवि कों और आकर्षित बनाते हैं। वर्तमान में कन्नौज नगर पालिका अध्यक्ष माननीय
इतिहास[संपादित करें]
आरंभिक इतिहास[संपादित करें]
पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि कन्नौज में चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड संस्कृति का निवास था,[5] क्रमशः ल. 1200-600 ईसा पूर्व और लगभग ल. 700-200 ईसा पूर्व। कुशस्थल और कान्यकुब्ज के नाम से, इसका उल्लेख हिंदू महाकाव्यों, महाभारत और रामायण में और व्याकरणविद् पतंजलि (ल. 150 ईसा पूर्व) द्वारा एक प्रसिद्ध शहर के रूप में किया गया है।[6] प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में कन्नौज का उल्लेख कन्नकुज्जा के रूप में किया गया है, और मथुरा से वाराणसी और राजगीर तक व्यापार मार्ग पर इसके स्थान का उल्लेख किया गया है।[7]
ग्रीको-रोमन सभ्यता में कन्नौज को कनागोजा या कनोगिजा के नाम से जाना जाता था, जो टॉलमी (ल. 140 ई.पू.) द्वारा भूगोल में दिखाई देता है। पाँचवीं और सातवीं शताब्दी में क्रमशः चीनी बौद्ध यात्रियों फ़ाहियान और ह्वेन त्सांग ने भी इसका दौरा किया था।[8]


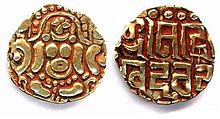
छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के दौरान, कन्नौज के मौखरी राजवंश - जिन्होंने गुप्तों के अधीन जागीरदार शासकों के रूप में कार्य किया था - ने केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का फायदा उठाया, अलग हो गए और उत्तरी भारत के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।[10]
मौखरियों के अधीन, कन्नौज का महत्व और समृद्धि बढ़ती रही। यह वर्धन राजवंश के सम्राट हर्ष (ल. 606 से 647 ई.) के अधीन उत्तरी भारत का सबसे महान शहर बन गया, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया।[11][12] चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और कन्नौज को कई बौद्ध मठों वाला एक बड़ा, समृद्ध शहर बताया।[13] हर्ष की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप महाराजा यशोवर्मन द्वारा कन्नौज के शासक के रूप में सत्ता हासिल करने तक सत्ता शून्य हो गई।[14]
कन्नौज त्रिभुज[संपादित करें]
8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच, कन्नौज तीन शक्तिशाली राजवंशों, अर्थात् गुज्जर-प्रतिहार (लगभग 730-1036 ई.), पाल (लगभग 750-1162 ई.) और राष्ट्रकूट (लगभग 753-982 ई.) का केंद्र बिंदु बन गया। तीन राजवंशों के बीच के संघर्ष को कई इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है।[15][16]

शुरुआती संघर्ष हुए लेकिन अंततः गुज्जर प्रतिहार शहर पर कब्ज़ा करने में सफल रहे।[15] गुज्जर-प्रतिहारों ने अवंती (उज्जैन पर आधारित) पर शासन किया, जो दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य और पूर्व में पाल साम्राज्य से घिरा था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुज्जर-प्रतिहार शासक वत्सराज (लगभग 780-800 ईस्वी) के हाथों इंद्रायुध की हार के साथ हुई।[15] पाल शासक धर्मपाल (ल. 770-821 ईस्वी) भी कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने का इच्छुक था, जिससे वत्सराज और धर्मपाल के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल की हार हुई।[17] अराजकता का लाभ उठाते हुए, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारवर्ष (जन्म 780-793 ई.) उत्तर की ओर बढ़े, वत्सराज को हराया और एक दक्षिण भारतीय शासक द्वारा सुदूर उत्तरी विस्तार को पूरा करते हुए, कन्नौज पर कब्ज़ा कर लिया।[16][18]
जब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष वापस दक्षिण की ओर बढ़ा, तो धर्मपाल को कुछ समय के लिए कन्नौज के नियंत्रण में छोड़ दिया गया। पालों और गुज्जर प्रतिहारों के दो उत्तरी राजवंशों के बीच संघर्ष जारी रहा: पाल के जागीरदार चक्रायुध (उज्जैन के लिए धर्मपाल के नामित) को प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय (राज. 805-833 ई.) ने हराया था, और कन्नौज पर फिर से गुज्जर प्रतिहारों का कब्जा हो गया था। धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्ज़ा करने की कोशिश की लेकिन मुंगेर में गुज्जर प्रतिहारों द्वारा बुरी तरह पराजित हो गया।[15] हालाँकि, नागभट्ट द्वितीय जल्द ही राष्ट्रकूट गोविंदा III (आर. 793-814 सीई) से हार गया, जिसने दूसरे उत्तरी उभार की शुरुआत की थी। एक शिलालेख में कहा गया है कि चक्रायुध और धर्मपाल ने गोविंदा तृतीय को गुज्जर प्रतिहारों के खिलाफ युद्ध के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनकी सहानुभूति जीतने के लिए धर्मपाल और चक्रायुध दोनों ने गोविंदा तृतीय के सामने समर्पण कर दिया। इस हार के बाद प्रतिहार शक्ति कुछ समय के लिए क्षीण हो गई। धर्मपाल की मृत्यु के बाद, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नुज पर पुनः कब्ज़ा कर लिया और इसे गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस अवधि के दौरान, राष्ट्रकूटों को कुछ आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था, और इसलिए उन्होंने, साथ ही पाल साम्राज्य ने, इसका विरोध नहीं किया।[15] इस प्रकार कन्नौज (9वीं शताब्दी ई.) पर कब्ज़ा करने के बाद गुज्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में सबसे बड़ी शक्ति बन गए।[15]
मध्ययुगीन काल[संपादित करें]
प्रसिद्ध पीर-ए-कामिल, हजरत पीर शाह जेवना अल-नकवी अल-बोखारी का जन्म भी 1493 में राजा सिकन्दर लोदी के शासनकाल में कन्नौज में हुआ था। वह जलालुद्दीन सुरख-पोश बुखारी के वंशज थे और उनके पिता सैयद सदर-उद-दीन शाह कबीर नकवी अल बुखारी एक महान संत थे और राजा सिकंदर लोधी के सलाहकारों में से भी थे। शाह ज्यूना शाह जीवना (उनके नाम पर एक शहर) में चले गए जो अब पाकिस्तान में है। कन्नौज में शाह ज्यूना के उपनिवेशित शहर:- सिराय-ए-मिरान, बिबियान जलालपुर, मखदुमपुर, लाल पुर (संत सैय्यद जलालुद्दीन हैदर सुरख पॉश बुखारी या लाल बुखारी के नाम से जुड़े)। उनके वंशज आज भी भारत और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं।[19][20][21][22]
गजनी के सुल्तान महमूद ने 1018 में कन्नौज पर कब्जा कर लिया। चंद्रदेव ने ल. 1090 कन्नौज में अपनी राजधानी के साथ गाहड़वाल वंश की स्थापना की। उनके पोते गोविंदचंद्र ने "कन्नौज को अभूतपूर्व गौरव तक पहुंचाया।" मोहम्मद ग़ोरी शहर के विरुद्ध आगे बढ़ा और 1193 के चंदावर का युद्ध में जयचंद्र को मार डाला।
अलबरूनी ने अन्य भारतीय शहरों की दूरी को समझाने के लिए "कन्नोज" को प्रमुख भौगोलिक बिंदु के रूप में संदर्भित किया है।[23] इल्तुतमिश की विजय के साथ "शाही कन्नौज का गौरव" समाप्त हो गया।[24]
17 मई 1540 को शेर शाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूँ को हराया।
औपनिवेशिक काल[संपादित करें]
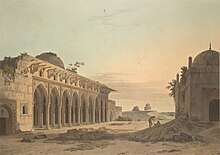
भारत में प्रारंभिक अंग्रेजी शासन के दौरान, उनके द्वारा शहर का नाम Cannodge(कैनौज) रखा जाता था।[25] नवाब हकीम मेहंदी अली खान उस समय के यात्रियों और लेखकों द्वारा लगातार कन्नौज शहर के विकास से जुड़े रहे हैं। एक घाट (मेहंदीघाट), एक सराय (यात्रियों और व्यापारियों के मुफ्त रहने के लिए) और विभिन्न पक्की सड़कें नवाब द्वारा बनवाई गईं, जिन पर उनका नाम भी है।
भूगोल[संपादित करें]
कन्नौज 27°04′N 79°55′E / 27.07°N 79.92°E पर स्थित है।[26] इसकी औसत ऊंचाई 139 मीटर (456 फीट) है।

जनसांख्यिकी[संपादित करें]
2001 की भारत की जनगणना के अनुसार,[27] कन्नौज की जनसंख्या 71,530 थी। जनसंख्या में 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। कन्नौज की औसत साक्षरता दर 58% है: पुरुष साक्षरता 64% है, और महिला साक्षरता 52% है। कन्नौज में 15% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है।
महाविद्यालय[संपादित करें]
चिकित्सा महाविद्यालय[संपादित करें]
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ से संबद्ध है।
इंजीनियरिंग महाविध्यालय[संपादित करें]
अहेर, तिर्वा में स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज डॉ॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ (पूर्व में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय) का घटक महाविद्यालय है।
परिवहन[संपादित करें]
शहर में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं-कन्नौज रेलवे स्टेशन और कन्नौज सिटी रेलवे स्टेशन। निकटतम हवाई अड्डा कानपुर हवाई अड्डा है जो शहर से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर स्थित है।
यह जीटी रोड (दिल्ली से कानपुर) पर स्थित है। इसमें सड़क परिवहन कन्नौज डिपो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के तहत।
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "Uttar Pradesh in Statistics," Kripa Shankar, APH Publishing, 1987, ISBN 9788170240716
- ↑ "Political Process in Uttar Pradesh: Identity, Economic Reforms, and Governance Archived 2017-04-23 at the वेबैक मशीन," Sudha Pai (editor), Centre for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, Pearson Education India, 2007, ISBN 9788131707975
- ↑ wink, Andre (2020). The Making of the Indo-Islamic World,C.700-1800 CE (अंग्रेज़ी में). Cambridge university press. पृ॰ 42.
- ↑ Hussain jafri, Saiyid Zaheer (2016). Recording the Progress of Indian History (अंग्रेज़ी में). Primus Books. पृ॰ 148.
- ↑ Dilip K. Chakrabarti (2007), Archaeological geography of the Ganga plain: the upper Ganga (Oudh, Rohilkhand, and the Doab), p.47
- ↑ Rama S. Tripathi, History of Kanauj: To the Moslem Conquest (Motilal Banarsidass, 1964), pp.2,15-16
- ↑ Moti Chandra (1977), Trade Routes in Ancient India pp.16-18
- ↑ Tripathi, History of Kanauj, pp. 17-19
- ↑ "CNG: eAuction 329. INDIA, Post-Gupta (Ganges Valley). Vardhanas of Thanesar and Kanauj. Harshavardhana. Circa AD 606-647. AR Drachm (13mm, 2.28 g, 1h)". www.cngcoins.com. मूल से 2 May 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 January 2019.
- ↑ Tripathi, History of Kanauj, pp. 22-24
- ↑ Tripathi, History of Kanauj, p. 147
- ↑ James Heitzman, The City in South Asia (Routledge, 2008), p.36
- ↑ Heizman, The City in South Asia, pp.36-37
- ↑ Tripathi, History of Kanauj, p. 192
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ Pratiyogita Darpan. Upkar Prakashan. पृ॰ 9. मूल से 8 March 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 November 2015.
- ↑ अ आ R.C. Majumdar (1994). Ancient India. Motilal Banarsidass. पपृ॰ 282–285. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-208-0436-4.
- ↑ Kumar Sundram (2007). Compendium General Knowledge. Upkar Prakashan. पृ॰ 195. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7482-181-2. मूल से 8 March 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 November 2015.
- ↑ Pratiyogita Darpan. Upkar Prakashan. मूल से 8 March 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 November 2015.
- ↑ "Pir-e-Kamil Hazrat Pir Shah Jewna Al-Naqvi Al-Bokhari". www.thenews.com.pk (अंग्रेज़ी में). मूल से 9 January 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-01.
- ↑ "Hazrat Pir Shah Jewna (RA)". The Nation (अंग्रेज़ी में). 2012-05-09. मूल से 2 September 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-01.
- ↑ "Indian Journal Of Archaeology". ijarch.org. मूल से 18 January 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-01.
- ↑ "Nazaria-i-Pakistan Trust". nazariapak.info. मूल से 3 August 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-01.
- ↑ (India, Vol 1, from p 199 onwards, Translated by Dr Edward C. Sachau, London 1910).
- ↑ Sen, S.N., 2013, A Textbook of Medieval Indian History, Delhi: Primus Books, ISBN 9789380607344
- ↑ Mrs. Meer Hassan Ali (1832). "Letter Nineteen". Observations on the Mussalmauns of India. मूल से 21 April 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 September 2022.
- ↑ "Falling Rain Genomics, Inc – Kannauj". मूल से 10 February 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 May 2007.
- ↑ "Census of India 2001: Data from the 2001 Census, including cities, villages and towns (Provisional)". Census Commission of India. मूल से 2004-06-16 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-11-01.


